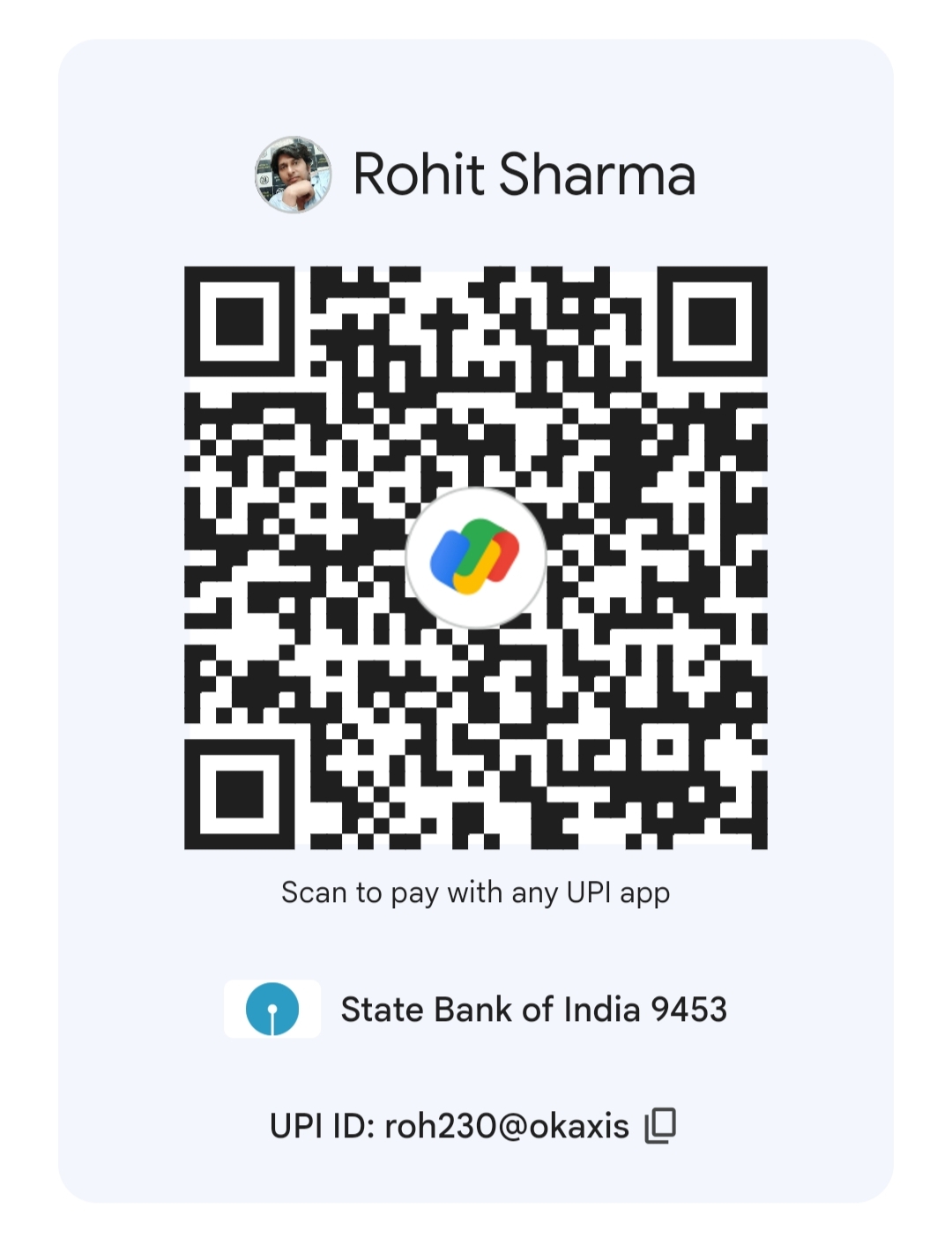क़ुरबान अली
देश में आजकल कुछ ‘समाजवादी’ इसराइल-फ़िलिस्तीन-अरब संघर्ष को लेकर काफ़ी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और इसराइल द्वारा किये जा रहे अरबों के नरसंहार की निंदा कर रहे हैं. साथ ही ये तथाकथित ‘सेक्युलर’ लोग यह तर्क भी दे रहे हैं कि ‘उनके नेता राममनोहर लोहिया ने 74 साल पहले जुलाई 1950 में इसराइल-अरब संघर्ष को लेकर जो चेतावनी दी थी, अगर उस समय उनकी बात मान ली गयी होती, तो आज पश्चिम एशिया में वैसा ख़ून-ख़राबा नहीं हो रहा होता, जो आज हो रहा है. और हैवानियत के सारे मंज़र आज दुनिया तमाशबीन बनकर देख रही है.
एक समाजवादी चिंतक प्रो. राजकुमार जैन ने अपने एक ताज़ा लेख में 1950 में दिए गए लोहिया के एक बयान को उद्धृत करते हुए लिखा है :
मैंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन गुरियन और अरब लीग के नेताओं की मीटिंग कराने की कोशिश की थी. इसराइल के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा था कि वे अरब नेताओं से मिलने के लिए कहीं भी जाने को तैयार हैं. मुझे लगा था कि सीमाओं की गारंटी तो प्रभावी की ही जा सकती है, हालांकि फिलिस्तीन के अरब शरणार्थियों की समस्या को हल करने में बहुत कठिनाई होगी.
किसी भी स्थिति में इस्राइल के लिए यह अच्छा होगा कि वह नाज़रेथ और अन्य स्थानों के अरबों को न केवल समान नागरिकता की औपचारिक सुविधा दें, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन की वह तमाम सुविधाएं भी दे, जो यहूदियों को दी जा रही है. मैं यह समझ नहीं पाया हूं कि अरबों और यहूदियों के लिए सामूहिक बस्तियां बनाने की पहल क्यों नहीं की जा सकती.
इस बीच मिस्र में चुनाव हुए हैं और मिलनसार नहास पाशा वहां प्रधानमंत्री बने हैं. मैंने जब 6 महीने पहले उनसे बात की थी, तो वह तीसरे खेमे के बारे में आशान्वित नहीं दिखे थे, लेकिन अगर भारत सकारात्मक नीति अपनाए, तो उनका मन भी बदल सकता है. जैसे भी हो नहास पाशा और आजम पाशा की बेन गुरियन से मीटिंग होनी चाहिए. इसका कुछ तो फायदा होगा, भले ही वह इसराइल-अरब युद्ध को न रोक पाए. भले ही कितने युद्ध हो जाएं, लेकिन अंततः समझौता तो होना ही चाहिए. इस तरह की बैठकें इसमें सहायक ही होती है. एक-न-एक दिन इसराइल और अरब दुनिया के बीच कुछ संघात्मक व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी.
अगर दुनिया में कहीं अंतिम व्यक्ति तक युद्ध करने जैसी भावना मुझे दिखी, तो वह इसराइल में ही दिखी. जब मैंने इसराइल के एक उत्साही नौजवान से कहा कि 8 करोड़ अरब शत्रुओं के सामने 20 लाख यहूदियों के टिके रहने की कोई संभावना नहीं है और किसी दिन अरबों के पास भी यहूदियों जितने हथियार आ जाएंगे, तो उसने अपने शांत उत्तर से मुझे डरा दिया. उसने कहा कि उनके लिए जाने की कोई जगह नहीं है.
आश्चर्य की बात है कि इस देश में जहां हर लड़की मशीनगन चला सकती है, महात्मा गांधी की आत्मकथा हर उस नौजवान ने पढ़ी है, जिससे मैं मिला. गहराई-गहराई को आमंत्रित करती है, चाहे वह हिंसक हो या अहिंसक. इसराइल एशियाई देश है. उसके पास इतने मानव संसाधन और प्रतिभाएं हैं कि किसी और देश में इतनी नहीं होगी. वह नए ढंग के जीवन के प्रयोग कर रहा है, विशेषकर कृषि में. शांति और पुनर्निर्माण के कार्य में इसराइल की साझेदारी सारे एशिया को, जिसमें अरब भी शामिल है, लाभान्वित करेगी.
भारत सरकार को इसराइल को मान्यता देने में देरी नहीं करनी चाहिए. मैं यही बात मिस्र की सरकार से भी कहना चाहता हूं. मैं यह बताने की जरूरत नहीं समझता कि मैंने मिस्र में अपने को ज्यादा घर जैसा सहज महसूस किया बनिस्बत इसराइल के लोगों के बीच, क्योंकि काहिरा में गंदगी, शोर और अनुशासनहीनता कानपुर की तरह ही है. यह दुःखों और उम्मीदों का रिश्ता और संभवत: दोनों देशों की संस्कृतियों का एक जैसा होना भी हमें एक दूसरे के करीब लाता है.
यह 1950 में इसराइल-अरब संघर्ष के बारे में राममनोहर लोहिया की राय थी. इतना ही नहीं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी व बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के ज़्यादातर नेता (दो-चार अपवादों को छोड़कर, जैसे राजनारायण और मधु लिमये) दरअसल इसराइल से ना सिर्फ़ हमदर्दी रखते थे, बल्कि इसराइल के पक्ष में ज़ोरदार ढंग से आंदोलन भी चलाते थे.
लोहिया के एक बहुत ही क़रीबी दोस्त अकबरपुर-फ़ैज़ाबाद के सिब्ते मोहम्मद नक़वी (वे उत्तर प्रदेश के पूर्व समाजवादी मंत्री और सांसद मुख़्तार अनीस के मामू और ससुर भी थे) ने 3 जुलाई 1967 को डॉ. लोहिया को एक ख़त लिखा. इस ख़त में उन्होंने लिखा कि :
जनाब डॉक्टर साहेब,
आपकी तरफ से अध्यात्म जी का 28 जून का, और आपका 30 जून का पत्र मुझे एक साथ मिला. बड़ी ख़ुशी हुई. मार खाना तो शायद मेरे भाग्य में आप से ज़्यादा है. (लोहिया ने अपने 30 जून के पत्र में लिखा था ‘प्रिय सिब्ते मुहम्मद, तुम्हारा ख़त ‘जन’ में पढ़ा. मुझे तो सब तरफ़ से मार खाना बदा है, तुम कहां तक बचाओगे’). मैं तो कभी-कभी ऐसा सोचता हूं कि शायद आप भी मुझे मार रहे हैं. सब्र तो इस ख़्याल से आता है कि मार तो हर उस आदमी को खानी पड़ेगी जो दो जीभें न कर सके….
कल या परसों के समाचार पत्रों में जॉर्ज फ़र्नांडिस साहब का मैंने इसराइल के पक्ष में एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर देखा और मुझे बड़ा दुःख हुआ. और आज जब ‘जन’ 28 मिला, तो वह दुःख और बढ़ा और मुझे खेद है कि इस क्रम में जो विचारधारा आपके द्वारा संसद में प्रतिपादित हुई है, उसे मैं ग़लत ही नहीं, अन्यायपूर्ण भी मानता हूं. गांधी जी ने 26 नवंबर 1938 के ‘हरिजन’ में एक लेख लिखा था, जिसके एक महत्वपूर्ण अंश का अनुवाद इस प्रकार है :
‘मेरी तमाम हमदर्दियां यहूदियों के साथ हैं, लेकिन हमदर्दियां न्याय के तक़ाज़ों से आंखें नहीं मुंदवा सकतीं. यहूदियों के लिए क़ौमी देश बनाने की चीख़ पुकार में मेरे लिए कोई अपील नहीं है. फ़िलस्तीन, अरबों की उसी तरह संपत्ति है, जैसे बर्तानिया अंग्रेज़ों की और फ़्रांस फ़्रांसीसियों की. यहूदियों को अरबों पर लादना ग़लत है.’
इस तरह अगर आप विचारेंगे, तो स्वयं आपको ‘अरब-इसराइल महासंघ’ की बात या इसराइल राज्य के अस्तित्व का स्वीकार आपको स्वयं न्यायसंगत नहीं दिखेगा. ‘अरब-इसराइल महासंघ’ की बात वैसी नहीं है जैसे हिंदुस्तान-पाकिस्तान, कोरिया और बर्लिन की है. इसराइल का अरब से वह रिश्ता है जो तिब्बत का चीन से. यह हमारी कमज़ोरी है कि शताब्दियां बीत जायें, हम तिब्बत को चीन के चंगुल से न निकाल सकें, लेकिन जब हम या खुद तिब्बत की जनता चीन की पाशविक बेड़ी तोड़ने के क़ाबिल हो जाये, उस वक़्त ‘जो हो गया सो हो गया’ को मान्यता देकर कहना कि अच्छा, चीन और तिब्बत का महासंघ बनवा दिया जाये, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे तो हरगिज़ अच्छा न लगेगा. हिटलर का रवैय्या यहूदियों के साथ बड़ी निर्दयता और बर्बरता का रहा है, लेकिन उनको बसाने के लिए अरब अपने घर से उजाड़े जाएं, इसका औचित्य मुझे तो नहीं दीखता. आप कृपया कर इस समस्या पर नए सिरे से ध्यान दें.
आशा है कि इस चिट्ठी से अगर आपको दुःख हो तो मुझे अपना मान के क्षमा करेंगे.
आपका
सिब्ते
राममनोहर लोहिया ने सिब्ते मुहम्मद के इस ख़त का जवाब 26 जुलाई 1967 को दिया :
प्रिय सिब्ते,
किसी हद तक तुमने ठीक ही लिखा है कि हर सुधार की दो शक्लें होती हैं, एक संभव और दूसरी सम्पूर्ण…
तुम को लग सकता है कि यकसां निजी क़ानून के मामले में, मैं शायद अति कर गया. ज़रा इस बात को भी सोचना कि महात्मा गांधी हिन्दू-मुसलमान के मामले में शायद थोड़ी कमी और मौक़ेबाज़ी कर गए. मुझे अक्सर मन में आता है कि मैं कितना बेवक़ूफ़ रहा कि हर मामले में किसी-न-किसी का विरोध करता रहा, जेल जाता रहा, लेकिन अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े ज़ुल्म और अन्याय, यानि बंटवारे के ख़िलाफ़ कुछ भी न कर पाया. इतना मौक़ेबाज़ बन गया, अपनी समझ के कारण नहीं, बल्कि उस ज़माने के नेताओं की मौक़ेबाज़ी के कारण.
जब तुर्की के मुसलमान ख़िलाफ़त ख़त्म कर रहे थे, तब हिंदुस्तान के मुसलमान और हिन्दू भी गांधी जी के नेतृत्व में ‘बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा ख़िलाफ़त पे दे दो’ गा रहे थे. पता नहीं, इन तरीक़ों से झुण्ड को इकठ्ठा कर लेना कितना अच्छा काम हुआ करता है …
तुमने इसराइल के बारे में गांधीजी का उद्धरण दिया है. मेरे बोलने और लिखने से उससे भी बड़े उद्धरण शायद निकल सकोगे. मैंने तो इसराइल को एशिया की छाती पर यूरोप का ख़ंजर कहा था. लेकिन अब सवाल पुरानी बातों का नहीं. अगर ऐसे ही पुरानी बातें उठाते रहोगे, तो फिर लोग कहना शुरू करेंगे कि ज्ञानवापी (वाराणसी) के पास मस्जिद को ठीक करके उसको पुरानी शकल में पहुंचाओ और मंदिर बनाओ, क्योंकि आखिर वहां मंदिर ही था. इतिहास की बहुत सी बातों को पचाना पड़ता है, लेकिन पचाने का ठीक मतलब समझना. आगे काम ठीक हो. पचने का यह मतलब नहीं कि जो कुछ हुआ, उसको सही मान लिया जाये, बल्कि यह कि जो कुछ हुआ, उस पर ग़ुस्सा न करके पछतावा करके ऊपर उठा जाये. तुमने जो मिसालें दी हैं, वो अगर ज़्यादा सोचोगे, तो तुम्हारी दृष्टि सुधरेगी. तिब्बत को स्वतंत्र करने का मतलब तिब्बत को ख़त्म करना नहीं होता. न भारत-पाकिस्तान के एके अथवा संघ से कोई ख़त्म होता है. और अगर ख़त्म भी होते हैं, तो दोनों ओर उसकी जगह हिंदुस्तान बनता है. उसी तरह से जब इसराइल के बारे में सोचोगे तो इसराइल को ख़त्म करने का मतलब समझना. आज के 22-23 लाख यहूदियों में से मैं समझता हूं. सब नहीं तो 15-20 लाख को मारे बिना इसराइल ख़त्म नहीं हो सकता. कहा कई क़ौमों ने है कि हम ख़ून की आख़िरी बूंद तक लड़ेंगे. इतिहास में अभी तक ऐसी कोई क़ौम नहीं हुई और शायद होगी भी नहीं लेकिन उसके पास तक पहुंचने वाली क़ौम अगर कोई होगी तो यही इसराइली. फिर जैसे-जैसे अरबी आधुनिक और शक्तिशाली होते जायेंगे, वैसे-वैसे उनका मन इसराइल के साथ संघ बनाने का होता जायेगा.
ख़त लिखते रहना.
तुम्हारा
राममनोहर लोहिया
इसके जवाब में सिब्ते मोहम्मद ने 30 जुलाई 1967 को डॉ. लोहिया को एक और लंबा ख़त लिखा. इस ख़त में उन्होंने लिखा :
जनाब डॉक्टर साहब,
… मुझे हरगिज़ यह नहीं लगता कि यकसां निजी क़ानून के मामले में आप ‘अति’ कर गए. मैंने कहना यह चाहा था कि जिस गति से आप ‘अति’ चाहते हैं, वो शायद अभी अव्यावहारिक और असंभव है… गांधी जी ने आपसे कम ज़्यादा आधी शताब्दी पहले का हिंदुस्तान देखा था… इसलिए मैं यह नहीं समझता कि इस मामले (हिन्दू-मुसलमान के मामले) में गांधी जी से कोई कमी हुई.
हिंदुस्तान-पाकिस्तान, वियतनाम, जर्मनी की परिस्थिति जो है, तिब्बत और इसराइल की उससे भिन्न है. वो एक थे, एक हैं. ताक़तवर स्वार्थियों ने उन्हें बांट कर अपना हित साधा. उनका एकीकरण या संघीकरण न्याय की बात है. जितनी जल्दी उसका वातावरण बन सके, उतना अच्छा है. मगर इसराइल में हिटलर के हाथों सताए हुए यहूदियों को बसाने के लिए फ़िलस्तीन में बसे हुए अरब बुरी तरह सताए और उजाड़े गए, जिनकी बहाली की कोई गंभीर कोशिश नहीं हुई. वो आज भी वैसे ही ‘ख़ानाबर्बाद’ है जैसे 30 साल पहले हुए थे. उनकी आबादकारी के सवाल को जोड़े बिना अरब-इसराइल समस्या का कोई हल ढूंढ़ना अन्यायसंगत होगा.
‘ज्ञानवापी’ और ‘बाबरी’ (मस्जिद) की बात सही हो सकती है. मैं उससे इंकार नहीं करता कि मंदिरों को मस्जिदों में परिवर्तित करने का कुकर्म नहीं किया गया. फिर भी आज कोई भी ऐतिहासिक तथ्य ऐसा नहीं है, जो परिवर्तनीय न हो…
इसराइल को अरब तो क्या पूरी तरह हिंदुस्तान ने भी मान्यता नहीं दी है. हमारा दूत-व्यवहार उनसे अब तक नहीं है. इसलिए यह मान कर चलना होगा कि उसका कोई अस्तित्व असंतोष और प्रतिरोध का विषय है और वह गई गुज़री बात की तरह पच नहीं सका है. मैं नहीं समझता कि इसराइल के वजूद को मिटा देने का मतलब कोई बीस लाख आदमियों को उजाड़ देना होगा. शायद इसका तात्पर्य यही हो कि उजड़े हुए फ़िलस्तीनी अरबों को भी नागरिकता की सुविधा मिले. इस जायज़ मांग की तरफ़ आंखें मूंद कर अंग्रेज़ और अमरीकी हल्क़े इसराइल के विस्तार के लिए और अरब-भूमि दिलाने की आवाज़ उठा रहे हैं, और स्वेज़ का साझीदार बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं. आपकी अरब-इसराइल नीति में अरब शरणार्थियों के पुनर्वास का हल जोड़ना ज़रूरी है.
इस तरह आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि इसराइल की समस्या तिब्बत ही जैसी है. वहां एक ख़ूंख़्वार क़ौम ने अपनी हद से बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिए एक शांतिप्रिय और दुर्बल जनसमूह का अपनी भूमि में सांस लेना दुर्लभ कर रखा है. आख़िर तिब्बत की आज़ादी का मतलब यही है ना कि वहां के असली बाशिंदे अपने ढंग से रह सकें और अपने देश की मनचाही व्यवस्था कर सकें. मेरी तुच्छ राय में इसराइल के अस्तित्व से इनकार का अर्थ यही है कि वहां के असली बाशिंदे भी अपनी मातृभूमि पर आज़ादी से रह सकें.
मैं तो आपसे सीखना और पाना इज़्ज़त और आबरू की बात समझता हूं. लेकिन मेरी बड़ी अदब के साथ यह प्रार्थना है कि आप अरब-इसराइल समस्या को फिर से परखें. मैं तो अपनी बेचैनी आप तक पहुंचा ही दिया करता हूं. आशा है, आप भी मेरे सुधार की तकलीफ़ सहते रहेंगे.
आपका
सिब्ते मोहम्मद
अकबरपुर, 30.07. 1967
इसके बाद राममनोहर लोहिया की ओर से सिब्ते मोहम्मद को कोई जवाब नहीं मिला. लोहिया के निजी सचिव अध्यात्म त्रिपाठी की ओर से केवल एक लाइन जवाब आया. आपका ख़त राममनोहर लोहिया को मिला, धन्यवाद. जब डॉक्टर साहब फ़र्रुख़ाबाद जायेंगे, उसकी सूचना हम आपको दे देंगे.’ (लोक सभा में लोहिया, खंड-15, पेज नंबर 234-242).
भारत के समाजवादियों ने कैसे इसराइल की मदद की ?
उपर मैंने अरब-इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया का दृष्टिकोण देखा था, यह प्रयास की बात थी. इस लेख में भारत के सोशलिस्टों की इजरायल के साथ दोस्ती और देशी-विदेशी मंचों पर उनके समर्थन का वोट डालने और उनके इजरायल के साथ हमजोली दास्तां की कोशिश की गई है.
महात्मा गांधी और समाजवादियों का दृष्टिकोण
बहुत कम लोगों को मालूम है कि महात्मा गांधी की आंखों के तारे कहे जाने वाले ‘समाजवादियों’ ने जो कांग्रेस पार्टी के अंदर ‘कांग्रेस सोशलिस्ट’ ब्लॉक के नाम से जाने जाते थे, 1948 में उनकी हत्या हो जाने के बाद फ़िलस्तीन मुद्दे पर महात्मा गांधी की घोषित नीति के ख़िलाफ़ जाकर इसराइल का समर्थन किया था.
इतना ही नहीं, इन महान ‘सेक्युलर’ और मानवतावादी लोगों ने इसराइल के साथ दोस्ताना और राजनयिक रिश्ते क़ायम करने की मुहिम भी चलायी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ‘सोशलिस्ट इंटरनेशनल’ के माध्यम से इसराइल को एक आतंकवादी देश बनने में मदद की.
इस लेख के पहले भाग में मैंने अरब-इसराइल-फ़िलस्तीन संघर्ष पर सोशलिस्ट नेता राममनोहर लोहिया का क्या नज़रिया था, यह बताने की कोशिश की थी. इस लेख में भारत के समाजवादियों की इसराइल के साथ दोस्ती और देशी-विदेशी मंचों पर उनके समर्थन का ब्यौरा देने और उनकी इसराइलों के साथ हमजोलियों की दास्तान बताने की कोशिश की गई है.
1948 के बाद का दौर : इसराइल का समर्थन
समाजवादियों का इसराइल प्रेम 1947 में उसके गठन के वक़्त से ही शुरू हो गया था, लेकिन गांधी जी की हत्या होने और औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी से अलग होने तक वह इस बारे में थोड़ा खामोश थे. इसराइल का दौरा करने और वहां कई-कई हफ़्तों तक ‘जायनिस्ट रिजीम’ की मेज़बानी उठाने वालों में भारत के शीर्ष समाजवादी नेताओं जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी, राममनोहर लोहिया, अशोक मेहता, एन जी गोरे, हरि विष्णु कामथ, प्रेम भसीन, नाथ पई, कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडीस, मधु दंडवते, सुरेंद्र मोहन, राजवंत सिंह, प्रदीप बोस, श्रीमती अनुसुईया लिमये, श्रीमती कमला सिन्हा आदि-आदि प्रमुख रूप से शामिल थे.
इसके अलावा इन नेताओं ने न सिर्फ़ इसराइल की आंतकवादी-विस्तारवादी नीतियों का समर्थन किया, बल्कि भारत सरकार पर इस बात के लिए भी दबाव डाला कि वह इसराइल के साथ न केवल राजनयिक रिश्ते क़ायम करे, बल्कि उसके साथ दोस्ताना सम्बन्ध भी बनाये.
जॉर्ज फर्नांडीस और ‘फ्रेंड्स ऑफ इसराइल’
संसोपा सांसद जॉर्ज फर्नांडीस ने तो जून 1967 में उस समय, जब इसराइल ने छह दिनों तक अरब देशों मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के साथ युद्ध करने और फ़िलस्तीन के एक बड़े भू-भाग पर नाजायज़ क़ब्ज़ा कर लिया था, भारत में ‘फ़्रेंड्स ऑफ़ इसराइल’ नामक संगठन बनाकर इसराइल की ‘जायनिस्ट रिजीम’ का समर्थन किया था.
इसराइल के समर्थन में उनका बयान न सिर्फ़ देश के बड़े अख़बारों में प्रमुखता के साथ छपा था, बल्कि राममनोहर लोहिया के संपादन में निकलने वाली पत्रिका ‘जन’ और ‘मैनकाइंड’ के जून 1967 के अंकों में प्रकाशित भी हुआ था.
जयप्रकाश नारायण का इसराइल दौरा
इससे पहले 1950 में राममनोहर लोहिया ने इसराइल का दौरा कर उसके लोगों और प्रगति की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी (देखें इस लेख का पहला भाग). सितम्बर 1958 में समाजवाद को तलाक़ देकर सर्वोदयी बने नेता जयप्रकाश नारायण ने इसराइल का दौरा किया और उन्होंने भी उसके लोगों और प्रगति की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी.
जेपी ने अपने इस इसराइल दौरे को बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हुए पूरी दुनिया से इसराइल के साथ सहयोग और दोस्ती की अपील की थी. साथ ही उन्होंने इसराइल का सामुदायिक कार्यक्रम ‘किबुत्ज़’ देखा और उससे वह अत्यंत प्रभावित हुए. (वाल्टर प्रीस -1960, पेज-160 और सर्वोदय पत्रिका, वॉल्यूम 8-9, पेज नंबर 339, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ़ जेपी)
इसके पहले जुलाई और अगस्त 1953 में कई एशियाई समाजवादियों ने ब्रिटेन का दौरा किया और स्टॉकहोम की सोशलिस्ट कांग्रेस में शिरकत की. इनमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त सचिव श्री प्रेम भसीन शामिल थे.
समाजवादियों ने इसराइल के साथ सहयोग और दोस्ती की बात संविधान सभा की बहसों के दौरान ही कर दी थी. फ़ॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हरि विष्णु कामथ, जो बाद में अपनी पार्टी के एक गुट का सोशलिस्ट पार्टी में विलय कर जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी और राममनोहर लोहिया के साथ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य बने, ने मार्च 1949 से दिसंबर 1949 के बीच कई बार संविधान सभा में इसराइल के साथ सहयोग का मुद्दा उठाया और हर बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट किया कि इसराइल के साथ सहयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि महात्मा गांधी के समय से हमारी नीति फ़िलस्तीन के साथ सहयोग की रही है, (सन्दर्भ : संविधान सभा की बहसें).
कांग्रेस पार्टी का इसराइल विरोध
इसराइल की स्थापना के पहले से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धार्मिक आधार पर इसराइल के गठन का विरोध कर रही थी. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता महात्मा गांधी का मानना था कि यहूदियों के साथ उनकी हमदर्दी है, लेकिन उन्होंने धार्मिक या अनिवार्य शर्तों पर इसराइल के निर्माण का विरोध किया.
गांधी का मानना था कि अरब फ़िलस्तीन के ‘सही मालिक’ थे, और उनका विचार था कि यहूदियों को अपने मूल देशों में लौट जाना चाहिए. गांधी जी ने 26 नवंबर, 1938 के ‘हरिजन’ में एक लेख लिखा था, जिसका एक महत्वपूर्ण अंश है :
‘मेरी तमाम हमदर्दियां यहूदियों के साथ हैं, लेकिन हमदर्दियां न्याय के तक़ाज़ों से आंखें नहीं मुंदवा सकतीं. यहूदियों के लिए क़ौमी देश बनाने की चीख़ पुकार में मेरे लिए कोई अपील नहीं है. फ़िलस्तीन, अरबों की उसी तरह संपत्ति है, जैसे बर्तानिया अंग्रेज़ों की और फ़्रांस फ़्रांसीसियों की. यहूदियों को अरबों पर लादना ग़लत है.’
मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भारत को यहूदी राज्य की स्थापना का समर्थन करने और उसे मनाने के लिए 13 जून 1947 को जवाहरलाल नेहरू को चार पन्नों का एक पत्र लिखा था. नेहरू ने आइंस्टीन के इस अनुरोध को विनम्रता के साथ अस्वीकार कर दिया. इतना ही नहीं, भारत ने 1947 की फ़िलस्तीन विभाजन योजना और संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के प्रवेश के ख़िलाफ़ भी मतदान किया.
हिंदू राष्ट्रवादियों का समर्थन
दूसरी ओर 1949 में हिंदू राष्ट्रवाद के विभिन्न समर्थकों ने इसराइल के निर्माण का समर्थन किया और उससे सहानुभूति व्यक्त की. हिंदू महासभा के नेता वी डी सावरकर ने नैतिक और राजनैतिक दोनों आधारों पर इसराइल के निर्माण का समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के खिलाफ भारत के वोट की निंदा की.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता माधव सदाशिव गोलवलकर ने यहूदी राष्ट्रवाद की प्रशंसा करते हुए कहा कि फ़िलस्तीन यहूदी लोगों का प्राकृतिक क्षेत्र है, जो राष्ट्रीयता की उनकी आकांक्षा के लिए आवश्यक है.
जबकि सोशलिस्ट नेता हरि विष्णु कामथ का कहना था कि अरबों के प्रति भारत की नीति अरबों से प्रेम के कारण नहीं, बल्कि राजनीति से प्रेरित है और इससे भारत का दोगलापन उजागर हुआ है. हरि विष्णु कामथ ने 17 अप्रैल, 1964 को लोकसभा में यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि भारत को अरब-इसराइल संघर्ष की तुलना में इसराइल के प्रति अपनी नीति अधिक सावधानी से बनानी चाहिए.
समाजवादियों की दोहरी नीति का विश्लेषण
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरएसएस और जनसंघ के अलावा इसराइल का खुला समर्थन करने वालों में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और स्वतंत्र पार्टी जैसे दल भी शामिल थे. भारतीय जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं को तो इसराइल में ट्रेनिंग भी दी जाती थी.
1950 के दशक में इसराइल की सत्ताधारी मापाई पार्टी (यह इसराइल की जायनिस्ट लेबर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी थी, जिसका विलय बाद में वहां की लेबर पार्टी में हो गया था) का भारत की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पीएसपी) के साथ घनिष्ठ संबंध रहा. पीएसपी और मापाई पार्टी के सदस्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोशलिस्ट इंटरनेशनल (एसआई) के साथ जुड़े थे.
जब इसराइल ने एशिया के अन्य देशों, ख़ासकर भारत के राजनीतिक दलों के साथ संबंध विकसित करना शुरू किये, तो इसकी शुरुआत जनवरी 1953 में रंगून में हुए पहले एशियाई समाजवादी सम्मेलन से हुई. इस एशियाई समाजवादी सम्मेलन में इसराइल को आमंत्रित किया गया था. (भारत और मध्य पूर्व, पृथ्वी राम मुडियाम – 1994 , पृष्ठ 153)
भारत में इसराइल के प्रति समाजवादियों का दृष्टिकोण
ग़ौरतलब बात यह है कि पीएसपी, एशियाई समाजवादी सम्मेलन को आयोजित करने वाली सह-प्रायोजित पार्टी थी और इससे इसराइल को एशिया में कुछ सम्मान हासिल करने और अपनी ज़मीन बनाने में मदद मिली. इस सम्मलेन में राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के अलावा भारत के 77 समाजवादी नेताओं ने भाग लिया था.
अक्टूबर-नवंबर 1956 में बम्बई में पीएसपी द्वारा आयोजित एशियन समाजवादियों के दूसरे सम्मेलन में इसराइल से मापाई पार्टी ने एक मजबूत प्रतिनिधिमंडल पूर्व प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोशे शेरेट के नेतृत्व में भारत भेजा.
इसके बाद मार्च 1966 में इसराइल के राष्ट्रपति ज़ल्मान शज़र काठमांडू के रास्ते कलकत्ता में थोड़े समय के लिए रुके, जहां समाजवादी नेताओं से उनकी मुलाक़ात हुई. उनकी इस यात्रा से एक बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ, क्यूंकि भारत सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी.
कलकत्ता में इस प्रकरण के बाद पीएसपी ने इसराइल से सामान्य संबंधों की वकालत तेज कर दी, जिसमें बाद में लोहिया की संसोपा भी शामिल हो गई. पीएसपी ने अक्टूबर 1966 में जारी अपने चुनाव घोषणापत्र में भी इसराइल के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने पर ज़ोर दिया और सरकार से इसराइल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का आग्रह किया. (जनता खंड-21, संख्या 39, 16 अक्टूबर, 1966 और पश्चिम एशिया और भारत की विदेश नीति, वरिंदर ग्रोवर द्वारा – 1992 – पृष्ठ-503).
1950 के दशक में ही सोशलिस्ट इंटरनेशनल ने, इसराइल के समाजवाद की उपलब्धियों की सराहना करते हुए एक आधिकारिक पुस्तिका भी प्रकाशित की, जिसमें प्रमुख भारतीय समाजवादी नेता, जेबी कृपलानी की प्रस्तावना शामिल थी, जिसमें उन्होंने इसराइली समाजवाद की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए इसराइल के बहिष्कार करने वालों की निंदा की थी, जिसमें भारत भी शामिल था. (फिलिप मेंडेस, निक डायरेनफर्थ – 2015)
वर्ष 1972 में प्रसोपा और संसोपा का विलय होने और सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो जाने के बाद बंबई में इसराइल श्रमिक नेताओं का एक उच्च पदस्थ प्रतिनिधिमंडल उप महासचिव सहित 20 अक्टूबर को हिंद मजदूर पंचायत कार्यालय के दफ़्तर में समाजवादी नेताओं से मिला, जिनमें इसराइल के बंबई स्थित उप-वाणिज्यदूत श्रीमान एवं श्रीमती जी. बेन-अमी भी शामिल थे.
इस दौरान इसराइली प्रतिनिधिमंडल ने भारत के समाजवादी नेताओं के साथ एक बैले नृत्य ‘आज़ादी की जंग’ का भी आनंद लिया. इस बैले नृत्य में 1857 से 1972 तक के भारत को गुलामी से आजादी की ओर ले जाने वाली शक्तियों और घटनाओं का चित्रण किया गया था. (जनता – खंड 27 – पृष्ठ 29, 1972)
27 से 29 अप्रैल, 1960 को इसराइल के शहर हाइफ़ा में सोशलिस्ट इंटरनेशनल की काउंसिल कांफ्रेंस की एक बैठक हुई. इस सम्मेलन में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष अशोक मेहता को आमंत्रित किया गया. ‘एशिया में सामाजिक लोकतंत्र के कार्य’ — इस विषय पर अशोक मेहता ने अपना शुरूआती भाषण दिया. (टास्क ऑफ़ सोशल डेमोक्रेसी इन एशिया पेज नंबर 1, अशोक मेहता)
उसी समय पीएसपी की ओर से पार्टी अध्यक्ष अशोक मेहता सोशलिस्ट इंटरनेशनल की रोम और वियना में हुई बैठकों में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी दौरा किया. (जनता – खंड 18 – पृष्ठ 414.1961).
1963 में पीएसपी पार्टी ने इसराइल को क़ानूनी मान्यता न देने के संबंध में केंद्र सरकार से सवाल किया. (‘इजरायल एंड द अरब्स’ सुरेंद्र मोहन, जनता, 8 अप्रैल 1964, भारत की विदेश नीति पर समाजवादियों का दृष्टिकोण – पृष्ठ 201, एस. एम. मोहिउद्दीन सुभानी – 1977).
इसके अलावा भारत-इजरायल सहयोग बढ़ाने और इसराइल के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता काफी सक्रिय और सबसे आगे थे. (भारत की इसराइल नीति, पी. आर. कुमारस्वामी द्वारा – 2013)
- क़ुरबान अली एक वरिष्ठ पत्रकार हैं. इस समय वे देश में समाजवादी आंदोलन के इतिहास का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं.
सन्दर्भ नोट
प्रथम एशियाई समाजवादी सम्मेलन (एशियन सोशलिस्ट) की बैठक 6 जनवरी, 1953 को रंगून में हुई. बैठक ने 15 जनवरी तक अपना विचार-विमर्श जारी रखा और इसमें 177 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. भारत, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, सियाम, वियतनाम, कोरिया, फिलीपींस, जापान, पाकिस्तान, लेबनान, मिस्र और इज़राइल से प्रतिनिधि आये थे. कुल 470 प्रतिनिधि थे. जयप्रकाश नारायण और अशोक मेहता के नेतृत्व में भारत का प्रतिनिधिमंडल शामिल था. सोशलिस्ट इंटरनेशनल का इतिहास- खंड 3 – पृष्ठ 367 ; जूलियस ब्रौन्थल – 1980 एवं प्रथम एशियाई समाजवादी सम्मेलन की रिपोर्ट, रंगून, 1953 – पृष्ठ 1).
यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र पर समाजवादी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क समिति : स्ट्रास्बका 7-9 मई 1960 ; पेरिस, 23 जुलाई 1960 : श्री एच. विल्सन, एम.पी., श्री एच. इर्नशॉ, श्री जे. क्लार्क के साथ थे एशियन सोशलिस्ट कांग्रेस के प्रतिनिधि श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री जगदीश सिंह, श्री रामा झा और श्री द्वारको सुंदरानी (सभी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से)
Read Also –
लोहिया और जेपी जैसे समाजवादियों ने अछूत जनसंघ को राजनीतिक स्वीकार्यता दी
नेहरु द्वेष की कुंठा से पीड़ित ‘मारवाड़ी समाजवाद’ ने लोहिया को फासिस्ट तक पहुंचा दिया
लोहिया को समझने की कोशिश
पेगासस और जनद्रोही सरकारें
[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लॉग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लॉग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]