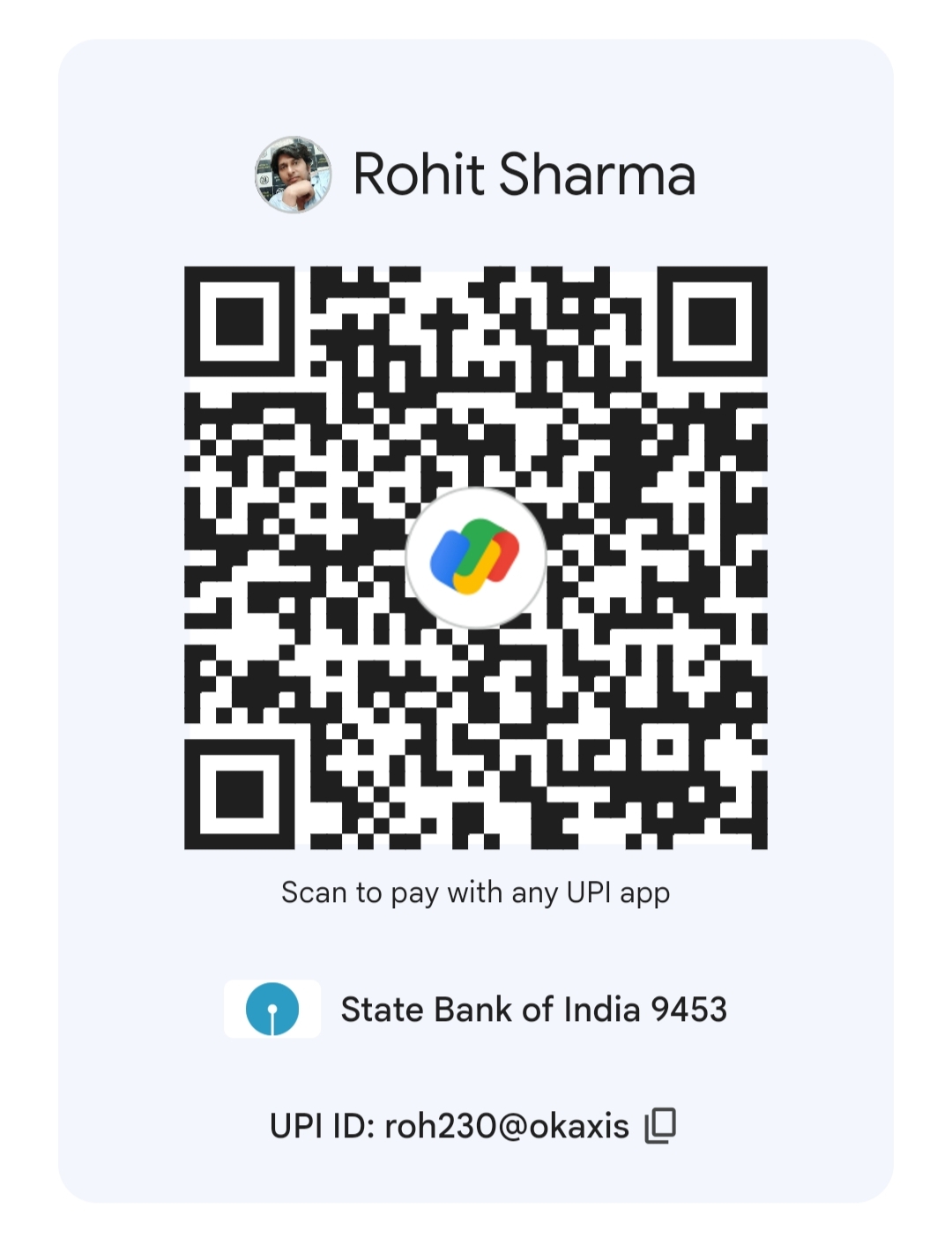दिल्ली में कम्युनिस्ट होना सरल है
बनिस्बत हमारे शहर के
और भी कठिन है,
हमारे जिले के किसी गांव के
दिल्ली में कम्युनिस्ट से कोई नहीं घबराता है
सोचते हैं कि कविता-वविता लिखता होगा
अकादमियों में भाषण देता होगा
शराब पी कर नारे लगाता होगा
तब इसे ज्यादातर लोग मत्त समझ कर
आगे बढ़ जाते होंगे
कम से कम कम्युनिस्ट नहीं समझते होंगे
सो,
वह एक सुरक्षित और आदरणीय घेरे में रहता है
और कम्युनिस्ट बना रहता है
बहुत फर्क है कॉमरेड,
हमारे जैसे छोटे शहर में
कम्युनिस्ट होना,
जहां परली गली तो क्या,
लगभग
सारी गलियों के लोग पहचानते हैं..
जब हारी हुई पार्टी होती है
तब तो वह विदूषक समझ लिया जाता है
लुंपेन, लंपट, दोगले,
जो कल उसे सलाम करते थे
दूर से हंसते हैं,
पास आ कर फुसफुसा कर दांत निपोर कर
चले जाते हैं,
उन्हें,
दिल्ली वालों की तरह पता नहीं होता
कि यह कविता भी लिखता है,
नाटक भी करता था
हमारे शहर में कम्युनिस्ट बने रहना ही
कम्युनिस्ट होना होता है
और भी मुश्किल है,
हमारे जिले के गांवों में जहां,
वह सच ही
कम्युनिस्ट हो जाता है,
होता जाता है,
क्योंकि उनमें से इक्का-दुक्कों नें ही
मार्क्स-लेनिन को पढ़ा होता है,
सो वे गुरबतों की ठोकरें खा कर,
मजलूमियत के धक्के खाते हुए
अपने शत्रु को पहचान लेते हैं
नारे लगाते हैं, जुलूसों में बढ़-चढ़ कर,
सोये बगैर ही
क्रांति के सपने देखते हैं और
अंत में संपत्ति के विवाद के बहाने
उनकी हत्या कर किसी पेड़-सा काट कर
खेत के किनारे फेंक दिए जाते हैं
तो महोदय,
आपको भी लगा ही होगा कि दिल्ली में
कम्युनिस्ट होना सरल तो है,
जबकि दिल्ली वालों को लगता है
कि उनके बगैर तो मार्क्स की हत्या ही हो जाती
- प्रमोद बेड़िया
[ प्रतिभा एक डायरी स्वतंत्र ब्लॉग है. इसे नियमित पढ़ने के लिए सब्सक्राईब करें. प्रकाशित ब्लॉग पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है. प्रतिभा एक डायरी से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर हैण्डल पर फॉलो करे… एवं ‘मोबाईल एप ‘डाऊनलोड करें ]